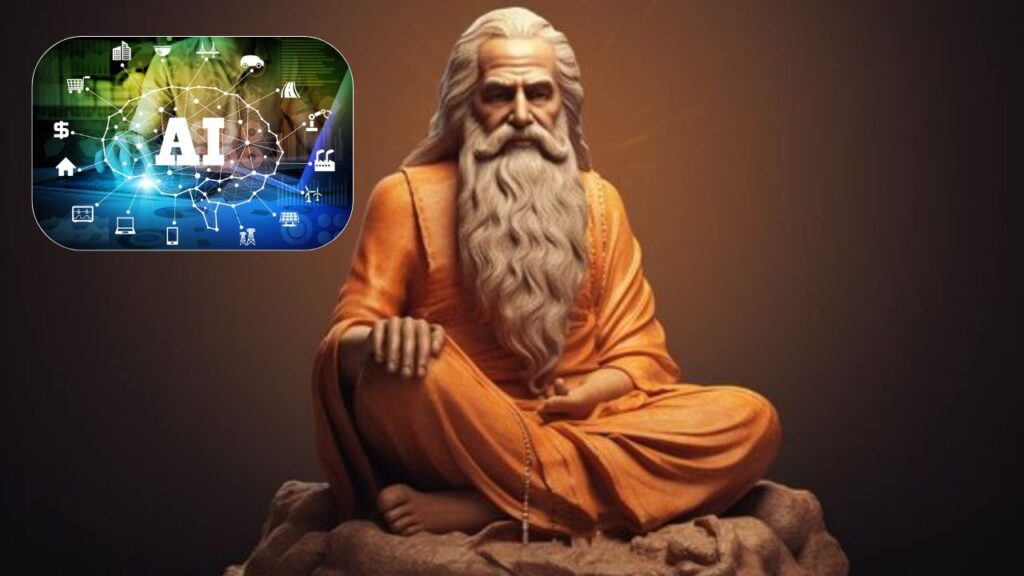#politicswala report
महर्षि वेद व्यास ने महाभारत, पुराणों और भारतीय ज्ञान-परंपरा को संरचित किया, वे गुरु परंपरा के मूल प्रतीक हैं। उनकी भूमिका मात्र ज्ञान देने की नहीं, बल्कि धर्म, नीति, चेतना और सामाजिक संतुलन स्थापित करने की थी। वहीं दूसरी ओर आज का युग एआई (Artificial Intelligence) का है जहाँ एक क्लिक करते ही ज्ञान का भंडार उपलब्ध है, लेकिन वह ज्ञान प्रेरणा नहीं बन पाता, दृष्टि नहीं देता, और जीवन का मार्गदर्शन नहीं करता। महर्षि वेद व्यास से लेकर एआई तक गुरु की भूमिका कैसे बदली? क्या बदलनी चाहिए? और क्या नहीं बदलनी चाहिए? इन प्रश्नों का उत्तर हमें उस संक्रमणकालीन यात्रा में मिलेगा जो व्यास से शुरू होती है और एआई तक पहुँचती है।
मुगल आक्रांता महमूद गजनवी के साथ 1017 में भारत आए अलबरूनी ने अपने संस्मरण ‘किताब-उल-हिन्द’ में लिखे। इसमें अलबरूनी ने लिखा कि मैंने अपने भारत-भ्रमण के दौरान वहाँ के हिंदुओं में तीन विशेषताएँ देखीं, पहला वहां का हिन्दू झूठ नहीं बोलता, दूसरा उसे अपनी मौत से डर नहीं लगता और तीसरा उसे अपनी ज्ञान परम्परा और शास्त्रों पर अगाध विश्वास है। हम सभी के अनुभव में भी आता है कि अब तीनों ही परिस्थितियां विपरीत हो चुकी हैं।
समाज में व्याप्त दुष्प्रवृत्तियों का आधिकारिक रूप से बीजारोपण 1835 में मैकाले ने अपनी विषाक्त शिक्षा प्रणाली के माध्यम से किया था। उसने अपनी शिक्षा नीति के माध्यम से समाज के मानस में ‘EEE’ (English, Education, Employment) फार्मूले को प्रतिस्थापित कर दिया, जिसके फलस्वरूप संस्कृत, संस्कार और गुरुकुल जैसी भारत की मूल शिक्षा परंपराएँ धीरे-धीरे अप्रासंगिक होती चली गईं। शिक्षा का उद्देश्य ‘युक्तकरी’ से हटकर केवल ‘नियुक्तिकरी’ बन गया। आज़ादी के बाद यह स्थिति और विकृत हो गई, मैकाले की सोच में मदरसे और मार्क्स की विचारधारा भी जुड़ गई, जिससे भारतीय समाज के ‘स्व’ का भाव विलोपित होता गया। इसका परिणाम यह हुआ कि समाज अपनी प्राचीन गौरवशाली परंपराओं को भूलकर हीनभावना से ग्रस्त हो गया।
भारत केवल एक भू-भाग नहीं, बल्कि अध्यात्म का पर्याय है। यदि भारत को पुनः भारत बनाना है, तो हमें अपनी हजारों वर्षों पुरानी जड़ों से जुड़ना होगा। इसके लिए गुरु-शिष्य परंपरा, संस्कृत, गुरुकुल, परिवार, समाज और शिक्षा इन सभी संस्थाओं का गहन परिष्कार अनिवार्य है। जब हर प्रश्न का उत्तर इंटरनेट और एआई से मिलने लगा है, तब गुरु की आवश्यकता पर प्रश्न खड़े होना स्वाभाविक है, परंतु इसके प्रत्युमत्तगर में यह भी स्पष्ट है कि एआई सूचना दे सकता है पर बोध नहीं, वह तथ्य बता सकता है किन्तुर सत्य का बोध नहीं करा सकता। एआई ज्ञान दे सकता है पर विवेक नहीं। गुरु तो ज्ञान को दृष्टि में बदलता है और दृष्टि को जीवन में उतारता है। एआई युग में गुरु की भूमिका अब चेतना के संरक्षक के रूप में और भी महत्वनपूर्ण हो गई है।
वर्तमान शिक्षा में चरित्र निर्माण का तत्व गौण हो गया है। बचपन से ही बच्चों को केवल प्रतिस्पर्धा, रैंक, करियर और सफलता की भाषा सिखाई जा रही है, जबकि संयम, सहनशीलता, आदर, विनम्रता जैसे मूल्य धीरे-धीरे लुप्त हो रहे हैं। गुरु की पुनर्प्रतिष्ठा की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि संस्कारों के बिना शिष्य गुरु को समझ नहीं सकता और बिना श्रद्धा के गुरु का प्रभाव नहीं बनता।
आज का छात्र शिक्षा को सेवा नहीं, बल्कि उत्पाद मानने लगा है। फीस देने के बाद ज्ञान का रिटर्न ऑन इन्वेोस्टेमेंट माँगने वाला समाज, गुरु को आचार्य नहीं, सेवाप्रदाता मान बैठा है। जब तक शिक्षा व्यभवसाय बनी रहेगी, तब तक छात्र और शिक्षक के बीच श्रद्धा का सेतु नहीं बन सकेगा। श्रद्धा तभी जागती है जब शिक्षक केवल ज्ञान नहीं, जीवन दर्शन भी साझा करता है।
गुरु बनने के लिए केवल पद नहीं, पात्रता चाहिए। वर्तमान समय में अधिकांश शिक्षक विषय विशेषज्ञ तो हैं, पर जीवन प्रशिक्षक एवं मार्गदर्शक नहीं बन पाए हैं। क्या शिक्षक आज भी विद्यार्थियों के भीतर मानवता का बीज बोते हैं? क्या वे केवल ‘टॉपर्स’ बनाने में लगे हैं, या चरित्रवान नागरिक भी बना रहे हैं? गुरु वही है, जो शिष्य के भविष्य को प्रतियोगिता में नहीं, बल्कि मूल्य में श्रेष्ठ बनाता है।
वर्तमान में युवा नौकरी की लालसा में छात्र की भूमिका में है और जीवन निर्वाह का सबसे आसान जरिया समझकर सूचना प्रदाता की आधी-अधूरी भूमिका का निर्वहन करने वाला व्यक्ति शिक्षक की भूमिका में है। छात्र के मन में न तो अपने शिक्षक के प्रति श्रद्धा है और न ही वह शिक्षा के मूल-उद्देश्य से परिचित है। जबकि, गुरु-शिष्य परंपरा केवल एक संस्थागत ढाँचा नहीं, बल्कि दो जीवंत चेतनाओं के बीच का संबंध है। जब व्यक्ति को अपने अज्ञान का ज्ञान हो जाता है तो उसके मन मे अनेक संशयों का जन्म होता है और वह उन संशयों के समाधान हेतु गुरु की तलाश प्रारम्भ करता है। शिष्यता एक साधना है और गुरुत्व एक तपस्या। इस संबंध की पुनर्स्थापना के बिना शिक्षा केवल सूचना बनकर रह जाएगी और समाज दिशा हीन हो जाएगा।
कुछ उपायों पर विशेष ध्यान देने की आवश्येकता है। नई शिक्षा नीति में मूल्य आधारित शिक्षा का समावेश केवल दस्तावेजों में नहीं बल्कि व्यावहार में होना चाहिए। शिक्षा संस्थानों में गोष्ठियों, चिंतन शिविर, चरित्र निर्माण के वर्गों की आवश्यकता है। संस्थानों में गुरु-शिष्यु का संवाद आत्मीय होना चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षण में आत्मिक अनुशासन भी अनिवार्य हो। समाज को यह समझना होगा कि शिक्षा विकास का उद्योग नहीं बल्कि संस्कारों का यज्ञ है। आज टेक्नोलॉजी के संयमित उपयोग की जरूरत है क्योंकि एआई औ डिजीटल टूल्स गुरु का विकल्प नहीं बल्कि सहायक हैं।
ऋषि वेद व्यास से एआई तक की यह यात्रा हमें सिखाती है कि ज्ञान का स्वरूप चाहे कितना भी बदले, उसके केंद्र में गुरु की आवश्यकता अपरिवर्तनीय है। आज जब समाज विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ऊँचाइयों को छू रहा है, वहीं मानवता और संवेदनशीलता की नींव डगमगा रही है। तकनीकी निर्भरता का यह युग हमें तेज़ी से सुविधा की ओर ले जा रहा है, लेकिन साथ ही आने वाली पीढ़ी का बौद्धिक विकास, विश्लेषण क्षमता और आत्मनिर्भर चिन्तन भी प्रभावित हो रहा है। अब शिशु अवस्था से ही मनुष्य केवल ‘टूल-ड्रिवन’ बनता जा रहा है, जो विचार करने के बजाय खोजने का आदी हो गया है। यह स्थिति केवल सामाजिक, सांस्कृतिक संकट का संकेत भी है। ऐसे में गुरु-शिष्य परंपरा ही सामाजिक स्थायित्व, नैतिक पुनर्जागरण और सांस्कृतिक पुनर्संस्कार दे सकती है। समाज के समग्र परिष्कार का मार्ग केवल वहीं से निकलेगा।
डॉ. संजय कुमार पाठक
(लेखक भारतीय शिक्षक मंडल के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख हैं)
You may also like
-
आज एक गिलास पानी मय्यसर नहीं और बातें 2047 के हिंदुत्व/हिंदुस्तान की
-
ममता ने अमित शाह को बताया ‘डकैत’, ईडी पर चोरी का केस
-
तेलंगाना .. के. कविता ने बनाई नई पार्टी, केसीआर की विरासत और हरीश राव को देंगी सीधी चुनौती
-
मां का जन्मदिन मनाने राबड़ी आवास पहुंचे तेजप्रताप, 7 महीने पहले हुए थे पार्टी परिवार से बेदखल
-
BJP मिशन 2026- Tamil Nadu में 4 जनवरी को Amit Shah का दौरा छेड़ेगा नए राजनीतिक तार